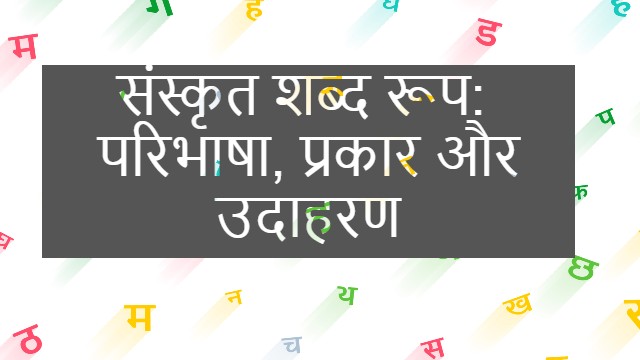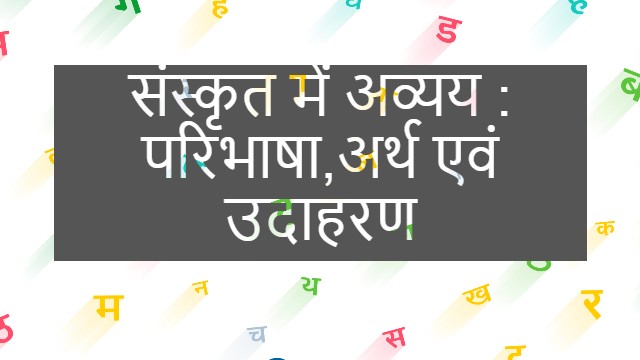संस्कृत में शब्द रूप
हिन्दी की तरह संस्कृत में भी शब्दों को निम्न प्रकार से पाँच भागों में बाँटा जा सकता है-
(१) संज्ञा, (२) सर्वनाम (३) विशेषण (४) क्रिया एवं (५) अव्यय ।
संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में लिंग तथा वचन के कारण तथा क्रिया में काल, पुरुष तथा वचन के कारण रूप परिवर्तन होता है, किन्तु अव्ययों में कभी परिवर्तन नहीं होता है।
प्रस्तुत प्रकरण में हम इन सबका संक्षेप में वर्णन करेंगे ।
सब्द रूप को समझने से पहले हमें संस्कृत में लिंग, वचन, पुरुष अदि के बारे में समझ लेना जरुरी है
संस्कृत भाषा में लिंग का विवरण (Gender in Sanskrit)
संस्कृत में तीन लिंग होते हैं-
(१) पुल्लिग, (२) स्त्रीलिंग एवं (३) नपुंसकलिंग ।
संस्कृत में लिंग का सम्बन्ध शब्दों से ही होता है, उन शब्दों के द्वारा व्यक्त होने वाले पदार्थों से नहीं होता। अतएव संस्कृत में लिंग निर्णय में विशेष कठिनौई होती है,
उदाहरणार्थ, ‘देवता’ शब्द के द्वारा व्यक्त पदार्थ पुल्लिंग का है, किन्तु संस्कृत में ‘देवता’ शब्द स्त्रीलिंग है। इसके विपरीत ‘पत्नी’ का अर्थ वाला ‘दारा’ शब्द पुल्लिंग है। हिन्दी में अग्नि और महिला शब्द स्त्रीलिंग हैं, किन्तु वे संस्कृत में पुल्लिग हैं। कभी-कभी तो लिंग भेद से शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है।
जैसे- मित्र’ शब्द पुल्लिग में सूर्य तथा नपुंसकलिंग में ‘सखा’ (friend) का अर्थ देता है।
यही नहीं एक अर्थ वाले विभिन्न शब्द भी अलग लिंगों में पाये जाते हैं। जैसे-बान्धव का समानार्थ मित्र नपुंसकलिंग है। इसी प्रकार भार्या के समानार्थ ‘दारा’ पुल्लिग, ‘पत्नी’ स्त्रीलिंग और ‘कलत्र’ नपुंसकलिंग है।
अतएव संस्कृत में लिंग का कार्य एक कठिन कार्य माना जाता है। इस पूर्ण ज्ञान के लिए कोष, व्याकरण तथा काव्य आदि का अध्ययन आवश्यक माना गया है। यद्यपि लिंग ज्ञान के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण नियम यहाँ देना असम्भव है फिर भी हम कुछ साधारण नियम लिख रहे हैं।
पुल्लिंग
१. ‘धञ्’ प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे-शोक, विहार, अनुपात आदि ।
२. इमनिच प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे-महिमा, गरिमा, लघिमा आदि ।
३. देवता (स्त्रीलिंग) शब्द को छोड़कर देवचाचक शब्द ‘रक्षस’ (नपुंसकलिंग) को छोड़कर असुर वाची शब्द तथा सुर और असुरों के नाम (पुल्लिंग) होते हैं। जैसे-अमरः, सुरः, देवः, विष्णुः, दानवः, असुरः, रावणः, बलिः आदि ।
४. यज्ञ वाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे-मखः क्रतुः, अध्वरः ।
५. पर्वतवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे-अद्रिः, गिरिः, शैलः।
६. समुद्रवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे- सागरः, समुद्रः, अब्धिः ।
७. अहन् तथा दिन (नपुंसकलिंग) को छोड़कर समय वाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे-मासः, वर्षः, पक्षः, दिवसः, कालः समयः ।
८. ‘अन्’ से समाप्त होने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे-राजन्, आत्मन् आदि ।
६. कि’ ‘अच्’ ‘अप्’ प्रत्यय युक्त शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे-विधि, निधिः, विजयः, विनय, करः, गजः, यशः ।
स्त्रीलिंग
१. आ, ई, ऊ से समाप्त होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे-रामा, लता, तरी, नदी, गौरी, वधू, तनु ।
२. क्तिन’ (ति) त् प्रत्यय से युक्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे-मतिः, यतिः, देवता, लघुता ।
३. विंशति से लेकर नवतिः तक संख्यावाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे-विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, नवतिः ।
नपुंसकलिंग
१. ‘त्व’ ‘ल्युट्’ (अन्) यत् (य) प्रत्यय वाले शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। जैसे-लघुत्वम, गुरुत्वम्, हितम्, सौकुमार्यम्, काठिन्यम् ।
२. क्रिया विशेषण भी नपुंसकलिंग होते हैं। जैसे सः शीघ्रं धावति । सीता मधुरं गायति ।
संस्कृत भाषा के वचन :
संस्कृत में तीन वचन होते हैं। एक के लिए एकवचन, दो के लिए द्विवचन और दो से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है।
उदाहरण:
- एकवचन (Singular) – एक व्यक्ति या वस्तु (e.g., बालकः = the boy)
- द्विवचन (Dual) – दो व्यक्ति या वस्तुएँ (e.g., बालकौ = two boys)
- बहुवचन (Plural) – तीन या अधिक व्यक्ति/वस्तुएँ (e.g., बालकाः = boys)
संस्कृत भाषा मे पुरुष
संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं-
(१) प्रथम पुरुष, (२) मध्यम पुरुष, (३) उत्तम पुरुष ।
त्वम् (तू या तुम), युवाम् (तुम दोनों), यूयम् (तुम सब) आदि, ‘युस्मद्’ शब्द के रूप में मध्यम पुरुष
तथा अहम् (मैं), आवाम् (हम दोनों), वयम् (हम सब) आदि ‘अस्मद्’ शब्द के रूपों में उत्तम पुरुष होते हैं।
इनके अतिरिक्त नाम सः (वह), तौ (वे दोनों), ते (वे सब) आदि ‘तद्’ शब्द के रूप में ‘भवान्’ (आप), भवन्तौ (आप दोनों) भवन्तः (आप सब) आदि ‘भवान्’ के रूप में तथा सा, ते, ता आदि प्रथम पुरुष होते हैं।
संज्ञा शब्द रूप
किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे- रामः बालकः, बालिका सौन्दर्यम् । संज्ञाओं में तीन लिंग, (पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग), तीनों वचन (एकवचन, द्विवचन और बहुवचन) तथा सम्पूर्ण विभक्तियाँ होती हैं और इनके कारण परिवर्तन होता है। कुछ शब्द अपने अन्त में स्वर रखते हैं, इन्हें अजन्त तथा स्वरान्त कहते हैं। जैसे-राम, कविता, लता ।
कुछ शब्द अपने अन्त में व्यंजन रखते हैं, इन्हें हलन्त या व्यंजनान्त कहते हैं, जैसे वणिक् ।
इन दोनों प्रकार के शब्दों में तीनों लिंग के शब्द रहते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण शब्दों को निम्न भागों में बाँटा जाता है, जिन्हें शब्दलिंग कहते हैं-
(१) अजन्त पुल्लिंग ।
(२) हलन्त पुल्लिंग ।
(३) अजन्त स्त्रीलिंग ।
(४) हलन्त स्त्रीलिंग ।
(५) अजन्त नपुंसकलिंग ।
(६) हलन्त नपुंसकलिंग ।
अकारान्त पुल्लिंग ‘बालक’ — लड़का
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | बालकः | बालकौ | बालकाः |
| द्वितीया | बालकम् | बालकौ | बालकान् |
| तृतीया | बालकेन | बालकाभ्याम् | बालकैः |
| चतुर्थी | बालकाय | बालकाभ्याम् | बालकेभ्यः |
| पंचमी | बालकात् | बालकाभ्याम् | बालकेभ्यः |
| षष्ठी | बालकस्य | बालकयोः | बालकानाम् |
| सप्तमी | बालके | बालकयोः | बालकेषु |
| संबोधन | हे बालक ! | हे बालकौ ! | हे बालकाः ! |
नोट: निम्न शब्दों के रूप भी बालक की तरह चलते हैं। केवल ‘र’ और ‘ष’ रखने वाले शब्दों के तृतीया एकवचन और षष्ठी बहुवचन में ‘न्’ की जगह ‘ण’ होता है। अतः ‘राम’ शब्द के तृतीया एकवचन में रामेण और षष्ठी बहुवचन में ‘रामाणाम्’ रूप बनेगें।
| संस्कृत शब्द | अर्थ (हिंदी) | संस्कृत शब्द | अर्थ (हिंदी) |
|---|---|---|---|
| रामः | राम | चौरः | चोर |
| जनकः | पिता | खरः | गधा |
| पुत्रः | पुत्र | सिंहः | शेर |
| छात्रः | विद्यार्थी | सर्पः | साँप |
| अश्वः | घोड़ा | शुकः | तोता |
| वानरः | बन्दर | चन्द्रः | चन्द्रमा |
| मयूरः | मोर | नृपः | राजा |
| खगः | पक्षी | गजः | हाथी |
| मनुष्यः | आदमी | कुक्कुरः | कुत्ता |
| सूर्यः | सूर्य | मृगः | हिरण |
| देवः | देवता | बुद्धः | विद्वान |
| करः | हाथ | — | — |
इकारान्त पुल्लिंग ‘मुनि’ — मुनि
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | मुनिः | मुनि | मुनयः |
| द्वितीया | मुनिम् | मुनि | मुनीन् |
| तृतीया | मुनिना | मुनिभ्याम् | मुनिभिः |
| चतुर्थी | मुनये | — | मुनये |
| पंचमी | मुन्यः | — | मुन्यः |
| षष्ठी | मुनेः | मुन्योः | मुनीनाम् |
| सप्तमी | मुनौ | मुन्योः | मुनीषु |
| सम्बोधन | हे मुनि ! | हे मुनि ! | हे मुनयः ! |
नीचे लिखे शब्दों के रूप भी मुनि की तरह ही चलते हैं।
केवल ‘र’ और ‘ण’ रखने वाले शब्दों के तृतीया एकवचन तथा षष्ठी बहुवचन में ‘न्’ की जगह ‘ण’ हो जायेगा तथा सप्तमी में ‘ष’ के स्थान पर ‘स’ हो जायेगा।
| संस्कृत शब्द | अर्थ (हिंदी) | संस्कृत शब्द | अर्थ (हिंदी) |
|---|---|---|---|
| अग्निः | आग | कविः | कवि |
| अरिः | शत्रु | ऋषिः | ऋषि |
| कपिः | बन्दर | निधिः | खजाना |
| हरिः | भगवान | गिरिः | पहाड़ |
| भूपतिः | राजा | रविः | सूर्य |
| विधिः | ब्रह्मा | यतिः | संन्यासी |
| जलधिः | समुद्र | — | — |
अपवाद — यद्यपि सभी इकारान्त पुल्लिंग शब्दों के रूप मुनि की तरह चलते हैं, किन्तु ‘सखि’ के रूप निम्न प्रकार से चलते हैं —
इकारान्त पुल्लिंग ‘सखि’ — मित्र
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | सखा | सखायौ | सखायः |
| द्वितीया | सखायम् | “ | सखीन् |
| तृतीया | सख्या | सखिभ्याम् | सखिभिः |
| चतुर्थी | सख्यै | “ | सखिभ्यः |
| पंचमी | सख्यः | “ | सखिभ्यः |
| षष्ठी | — | सख्योः | सखीनाम् |
| सप्तमी | सख्यौ | “ | सखिषु |
| सम्बोधन | हे सखे ! | हे सखायौ ! | हे सखायः ! |
उकारान्त पुल्लिंग ‘शिशु’ — छोटा लड़का
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | शिशुः | शिशू | शिशवः |
| द्वितीया | शिशुम् | “ | शिशून |
| तृतीया | शिशुना | शिशुभ्याम् | शिशुभिः |
| चतुर्थी | शिशवे | “ | शिशुभ्यः |
| पंचमी | “ | “ | शिशुभ्यः |
| षष्ठी | शिशोः | शिश्वोः | शिशूनाम् |
| सप्तमी | शिशौ | शिश्वोः | शिशुषु |
| सम्बोधन | हे शिशु ! | हे शिशु ! | हे शिशवः ! |
निम्न उकारान्त पुल्लिंग शब्दों के रूप भी शिशु के समान चलते हैं।
केवल ‘र’ और ‘अ’ रखने वाले शब्दों के तृतीया एकवचन तथा षष्ठी बहुवचन में ‘न्’ की जगह ‘ण’ रहेगा। ‘धेनुः’ शब्द के रूपों में केवल द्वितीया बहुवचन में धेनून न होकर ‘धेनूः’ बनेगा।
| संस्कृत शब्द | अर्थ (हिंदी) | संस्कृत शब्द | अर्थ (हिंदी) |
|---|---|---|---|
| भानुः | सूर्य | तरुः | वृक्ष |
| ऊरुः | जाँघ | गुरुः | गुरु |
| साधुः | सज्जन | विदुः | चन्द्रमा |
| वायुः | हवा | मृत्यु | मौत |
| मृदुः | कोमल | पशुः | जानवर |
| ईशुः | बाण | प्रभुः | भगवान, स्वामी |
सम्बन्धवाचक ऋकारान्त पुल्लिंग ‘पितृ’ — पिता
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | पिता | पितरौ | पितरः |
| द्वितीया | पितरम् | पितरौ | पितृन् |
| तृतीया | पित्रा | पितृभ्याम् | पितृभिः |
| चतुर्थी | पित्रे | पितृभ्याम् | पितृभ्यः |
| पंचमी | पितुः | पितृभ्याम् | पितृभ्यः |
| षष्ठी | पितुः | पित्रोः | पितृणाम् |
| सप्तमी | पितरि | पित्रोः | पितृषु |
| सम्बोधन | हे पितः ! | हे पितरौ ! | हे पितरः ! |
विशेष — स्त्रीलिंग मातृ के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं। केवल द्वितीया बहुवचन में मातृन् न होकर मातृः होता है। मातृ के रूप पितृ की तरह ही चलेंगे।
तकारण्त पुल्लिंग ‘भगवत्’
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | भगवान् | भगवन्तौ | भगवन्तः |
| द्वितीया | भगवन्तम् | “ | भगवन्तः |
| तृतीया | भगवता | भगवद्भ्याम् | भगवद्भिः |
| चतुर्थी | भगवते | “ | भगवद्भ्यः |
| पंचमी | भगवतः | “ | भगवद्भ्यः |
| षष्ठी | भगवतः | भगवतोः | भगवतः |
| सप्तमी | भगवति | भगवतोः | भगवति |
| सम्बोधन | हे भगवन् ! | हे भगवन्तौ ! | हे भगवन्तः ! |
विशेष—
- भवत् (आप), श्रीमत् (श्रीमन्त), विद्यावत् (विद्वान्) आदि शब्दों के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं।
- भगवत्, भवत्, श्रीमन् आदि शब्दों के स्त्रीलिंग में भगवती, भवती, श्रीमती आदि बनते हैं और इनके रूप नदी की तरह चलते हैं।
तकारान्त पुल्लिंग ‘महत्’—महान्
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | महान् | महान्तौ | महान्तः |
| द्वितीया | महान्तम् | महान्तौ | महतः |
| तृतीया | महता | महद्भ्याम् | महद्भिः |
| चतुर्थी | महते | महद्भ्याम् | महद्भ्यः |
| पंचमी | महतः | महद्भ्याम् | महद्भ्यः |
| षष्ठी | महतः | महतोः | महताम् |
| सप्तमी | महति | महतोः | महत्सु |
| सम्बोधन | हे महत्त ! | हे महन्तौ ! | हे महान्तः ! |
नकारान्त पुल्लिंग ‘राजन्’—राजा
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | राजन् | राजानौ | राजानः |
| द्वितीया | राजानम् | राजानौ | राज्ञः |
| तृतीया | राज्ञा | राजभ्याम् | राजभिः |
| चतुर्थी | राज्ञे | राजभ्याम् | राजभ्यः |
| पंचमी | राज्ञः | राजभ्याम् | राजभ्यः |
| षष्ठी | राज्ञः | राज्ञोः | राजाम् |
| सप्तमी | राज्ञि, राजनि | राज्ञोः | राजसु |
| सम्बोधन | हे राजन् ! | हे राजानौ ! | हे राजानः ! |
अकारान्त स्त्रीलिंग ‘बालिका’—लड़की
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | बालिका | बालिके | बालिकाः |
| द्वितीया | बालिकाम् | बालिके | बालिकाः |
| तृतीया | बालिकया | बालिकाभ्याम् | बालिकाभिः |
| चतुर्थी | बालिकायै | बालिकाभ्याम् | बालिकाभ्यः |
| पंचमी | बालिकायाः | बालिकाभ्याम् | बालिकाभ्यः |
| षष्ठी | बालिकायाः | बालिकयोः | बालिकानाम् |
| सप्तमी | बालिकायाम् | बालिकयोः | बालिकासु |
| सम्बोधन | हे बालिके ! | हे बालिके ! | हे बालिकाः ! |
अत्र शब्दों के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं (केवल ‘र’ और ‘अ’ रखने वाले शब्दों में षष्ठी बहुवचन में ‘न’ के स्थान पर ‘ण’ हो जाता है)
| संस्कृत शब्द | अर्थ (हिंदी) | संस्कृत शब्द | अर्थ (हिंदी) |
|---|---|---|---|
| उमा | पार्वती | नासिका | नाक |
| गंगा | गंगा | लता | बेल |
| अश्वा | घोड़ी | रमा | लक्ष्मी |
| विद्या | विद्या | बाला | कन्या |
| कान्ता | पत्नी | सुता | पुत्री |
| कलिका | कली | शिखा | चोटी |
ईकारान्त स्त्रीलिंग ‘मति’ – बुद्धि
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | मति | मती | मतयः |
| द्वितीया | मतिम् | मती | मतिः |
| तृतीया | मत्या | मतिभ्याम् | मतिभिः |
| चतुर्थी | मतये, मतौ | मतिभ्याम् | मतिभ्यः |
| पंचमी | मतयाः, मतोः | मतिभ्याम् | मतिभ्यः |
| षष्ठी | मतयाः, मतोः | मत्योः | मतीनाम् |
| सप्तमी | मत्याम्, मतौ | मत्योः | मतिषु |
| सम्बोधन | हे मते ! | हे मती ! | हे मतयः ! |
गति (चाल), बुद्धि, श्रद्धि आदि ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्द के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं।
ईकारान्त स्त्रीलिंग ‘नदी’
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | नदी | नद्यौ | नद्यः |
| द्वितीया | नदīm | नद्यौ | नदी: |
| तृतीया | नद्या | नदीभ्याम् | नदीभिः |
| चतुर्थी | नद्यै | नदीभ्याम् | नदीभ्यः |
| पंचमी | नद्याः | नदीभ्याम् | नदीभ्यः |
| षष्ठी | नद्याः | नद्योः | नदीनाम् |
| सप्तमी | नद्याम् | नद्योः | नदीषु |
| सम्बोधन | हे नदि ! | हे नद्यौ ! | हे नद्यः ! |
निम्न शब्दों के रूप भी इसी प्रकार चलेंगे –
| संस्कृत शब्द | अर्थ (हिंदी) | संस्कृत शब्द | अर्थ (हिंदी) |
|---|---|---|---|
| पार्वती | पार्वती | राड़ी | रानी |
| रजनी | रात्रि | मही, पृथ्वी | ज़मीन |
| जननी | माता | पत्नी | भार्या |
| देवी | देवी | दासी | नैकरानी |
| भगिनी | बहिन | नारी | स्त्री |
| कुमारी | अविवाहित स्त्री | कुटी | झोंपड़ी |
हलन्त स्त्रीलिंग शब्द चकारान्त – ‘वाच्’ (वाणी)
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | वाक्, वाग् | वाचौ | वाचः |
| द्वितीया | वाचम् | वाचौ | वाचः |
| तृतीया | वाचा | वाग्भ्याम् | वाग्भिः |
| चतुर्थी | वाचे | वाग्भ्याम् | वाग्भ्यः |
| पंचमी | वाचः | वाग्भ्याम् | वाग्भ्यः |
| षष्ठी | वाचः | वाचोः | वाचाम् |
| सप्तमी | वाचि | वाचोः | वाक्षु |
| संबोधन | हे वाक्, हे वाग्! | हे वाचौ! | हे वाचः! |
निम्न शब्दों के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं –
- रूप (रुक्) = कांति
- शुच् (शुच्) = जौंक
- स्रज (स्रक्) = माला
- ऋच् (ऋक्) = ऋचा
तकारण्त स्त्रीलिंग ‘सरित्’ – नदी
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | सरित् | सरितौ | सरितः |
| द्वितीया | सरितम् | सरितौ | सरितः |
| तृतीया | सरिता | सरिद्भ्याम् | सरिद्भिः |
| चतुर्थी | सरिते | सरिद्भ्याम् | सरिद्भ्यः |
| पंचमी | सरितः | सरिद्भ्याम् | सरिद्भ्यः |
| षष्ठी | सरितः | सरितोः | सरिताम् |
| सप्तमी | सरिति | सरितोः | सरितिषु |
| संबोधन | हे सरित्! | हे सरितौ! | हे सरितः! |
अकारान्त नपुंसकलिंग ‘फल’
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | फलम् | फले | फलानि |
| द्वितीया | फलम् | फले | फलानि |
| तृतीया | फलेन | फलाभ्याम् | फलैः |
| चतुर्थी | फलाय | फलाभ्याम् | फलाभ्यः |
| पंचमी | फलात् | फलाभ्याम् | फलाभ्यः |
| षष्ठी | फलस्य | फलयोः | फलानाम् |
| सप्तमी | फले | फलयोः | फलिषु |
| संबोधन | हे फल! | हे फले! | हे फलानि! |
निम्न शब्दों के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं —
| संस्कृत शब्द | हिन्दी अर्थ | संस्कृत शब्द | हिन्दी अर्थ |
|---|---|---|---|
| पुष्पम्, कुसुमम् | फूल | जलम् | पानी |
| वनम् | वन | पुस्तकम् | पुस्तक |
| वस्त्रम् | कपड़ा | उपवनम् | बगीचा |
| मित्रम् | मित्र | नगरम् | नगर |
| पत्रम् | पत्र | नेत्रम् | आँख |
| कमलम् | कमल | पात्रम् | पात्र |
| उद्यानम् | बगीचा | मुखम् | मुख |
| धनम् | धन | सुखम् | सुख |
| दुःखम् | दुःख | शरीरम् | शरीर |
इकारान्त नपुंसकलिंग ‘वारि’
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | वारि | वारिणी | वारिणि |
| द्वितीया | वारि | वारिणी | वारिणि |
| तृतीया | वारिणा | वारिभ्याम् | वारिभिः |
| चतुर्थी | वारिणे | वारिभ्याम् | वारिभ्यः |
| पंचमी | वारिणः | वारिभ्याम् | वारिभ्यः |
| षष्ठी | वारिणः | वारिणोः | वारिणाम् |
| सप्तमी | वारिणि | वारिणोः | वारिषु |
| संबोधन | हे वारि! | हे वारिणी! | हे वारिणि! |
तकारान्त नपुंसकलिंग ‘जगत्’ — संसार
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | जगत् | जगती | जगन्ति |
| द्वितीया | जगत् | जगती | जगन्ति |
| तृतीया | जगता | जगद्भ्याम् | जगद्भिः |
| चतुर्थी | जगते | जगद्भ्याम् | जगद्भ्यः |
| पंचमी | जगतः | जगद्भ्याम् | जगद्भ्यः |
| षष्ठी | जगतः | जगतोः | जगताम् |
| सप्तमी | जगति | जगतोः | जगत्सु |
| संबोधन | हे जगत्! | हे जगती! | हे जगन्ति! |
सकारान्त नपुंसकलिंग ‘मनस्’ — मन
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | मनः | मनसी | मनांसि |
| द्वितीया | मनः | मनसी | मनांसि |
| तृतीया | मनसा | मनोभ्याम् | मनोभिः |
| चतुर्थी | मनसे | मनोभ्याम् | मनोभ्यः |
| पंचमी | मनसः | मनसोः | मनसाम् |
| षष्ठी | मनसः | मनसोः | मनसाम् |
| सप्तमी | मनसि | मनसोः | मनस्सु, मनसु |
| संबोधन | हे मनः ! | हे मनसी ! | हे मनांसि ! |
निम्न शब्दों के रूप भी इसी प्रकार चलते हैं—
| संस्कृत शब्द | हिन्दी अर्थ | संस्कृत शब्द | हिन्दी अर्थ |
|---|---|---|---|
| पयस् | जल, दूध | वयस् | उम्र |
| नभस् | आकाश | वक्षस् | छाती |
| रजस् | धूल | सरस् | तालाब |
| यशस् | यश | वचस् | वचन |
| तपस् | तपस्या |
सर्वनाम शब्द रूप
जो शब्द संज्ञाओं की जगह प्रयोग किये जाते हैं, वे सर्वनाम कहे जाते हैं, जैसे—सर्व, सा, किम आदि।
नियम: सभी सर्वनाम शब्द रूप एक समान चलते हैं। इनमें तीनों लिंग होते हैं। प्रयोग के अनुसार ये विशेषण भी हो जाते हैं।
सर्व (सप्त) पुल्लिंग
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | सर्वः | सर्वौ | सर्वे |
| द्वितीया | सर्वम् | सर्वौ | सर्वान् |
| तृतीया | सर्वेण | सर्वाभ्याम् | सर्वैः |
| चतुर्थी | सर्वाय | सर्वाभ्याम् | सर्वेभ्यः |
| पञ्चमी | सर्वात् | सर्वाभ्याम् | सर्वेभ्यः |
| षष्ठी | सर्वस्य | सर्वयोः | सर्वेषाम् |
| सप्तमी | सर्वस्मिन् | सर्वयोः | सर्वेषु |
नोट— सर्वनामों में नपुंसकलिंग में प्रथमा तथा द्वितीया को छोड़कर अन्य सभी रूप समान होते हैं।
सर्व (नपुंसकलिंग)
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | सर्वम् | सर्वे | सर्वाणि |
| द्वितीया | सर्वम् | सर्वे | सर्वाणि |
सर्व (स्त्रीलिंग)
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | सर्वा | सर्वे | सर्वाः |
| द्वितीया | सर्वाम् | सर्वे | सर्वाः |
| तृतीया | सर्वया | सर्वाभ्याम् | सर्वाभिः |
| चतुर्थी | सर्वायै | सर्वाभ्याम् | सर्वाभ्यः |
| पञ्चमी | सर्वायाः | सर्वाभ्याम् | सर्वाभ्यः |
| षष्ठी | सर्वायाः | सर्वयोः | सर्वासाम् |
| सप्तमी | सर्वायाम् | सर्वयोः | सर्वासु |
युष्मद्, अस्मद् को छोड़कर प्रायः सभी सर्वनामों के रूप एक से ही चलते हैं,
किन्तु छात्रों की सुविधा के लिये उन्हें लिखा जा रहा है। अनुवादोपयोगी रूपों की हिंदी भी साथ दी जा रही है।
तद् (वह) पुल्लिंग
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | सः (वह) | तौ (वे दोनों) | ते (वे सब) |
| द्वितीया | तम् (उसको) | तौ (उन दोनों को) | तान् (उनको) |
| तृतीया | तेन (उससे) | ताभ्याम् (उन दोनों से) | तैः (उनसे या द्वारा) |
| चतुर्थी | तस्मै (उसके लिए) | ताभ्याम् (उन दोनों के लिए) | तेभ्यः (उनके लिये) |
| पञ्चमी | तस्मात् (उससे) | ताभ्याम् (उन दोनों से) | तेभ्यः (उनसे) |
| षष्ठी | तस्य (उसका) | तयोः (उन दोनों का) | तेषाम् (उनका) |
| सप्तमी | तस्मिन् (उस पर) | तयोः (उन दोनों पर) | तेषु (उन पर) |
नोट— तद् नपुंसकलिंग के रूप प्रथमा एवं द्वितीया को छोड़कर शेष पुल्लिंग के समान ही होते हैं।
तद् (वह) नपुंसकलिंग
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | तत् | ते | तानि |
| द्वितीया | तत् | ते | तानि |
तद् (स्त्रीलिंग)
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | सा | ते | ताः |
| द्वितीया | ताम् | ते | ताः |
| तृतीया | तया | ताभ्याम् | ताभिः |
| चतुर्थी | तस्यै | ताभ्याम् | ताभ्यः |
| पञ्चमी | तस्याः | “ | ताभ्यः |
| षष्ठी | तस्याः | “ | तासाम् |
| सप्तमी | तस्याम् | तयोः | तासु |
‘तद्’ शब्दों के रूप में आगे ‘ए’ लगा देने से ‘एतद्’ के रूप बन जाते हैं, जैसे—
एतद् (यह) पुल्लिंग
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | एषः (यह) | एषौ (ये दोनों) | एते (ये सब) |
| द्वितीया | एतम्, एनम् (इनको) | एतौ, एनी (इन दोनों को) | एतान् (इनको) |
| तृतीया | एतेन (इसने) | एताभ्याम् (इन दोनों ने) | एतैः (इनोंने) |
| चतुर्थी | एतस्मै (इसके लिए) | एताभ्याम् (इन दोनों के लिए) | एतेभ्यः (उनके लिए) |
| पञ्चमी | एतस्मात् (इससे) | एताभ्याम् (इन दोनों से) | एतेभ्यः (इनसे) |
| षष्ठी | एस्य (इसका) | एतयोः (इन दोनों का) | एतेषाम् (इनका) |
| सप्तमी | एस्मिन (इस पर) | एतयोः (इन दोनों पर) | एतेषु (इन पर) |
एतद् (यह) नपुंसकलिंग
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | एतत् | एते | एतानि |
| द्वितीया | ” | ” | एतानि |
| शेष पुल्लिंग की तरह |
एतद् (यह) स्त्रीलिंग
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | एषा | एते | एताः |
| द्वितीया | एताम् | एते | एताः |
| तृतीया | एया | एताभ्याम् | एताभिः |
| चतुर्थी | एस्यै | ” | एताभ्यः |
| पञ्चमी | एस्याः | ” | ” |
| षष्ठी | ” | एतयोः | एतासाम् |
| सप्तमी | एस्याम् | एतयोः | एतासु |
टिप्पणी:
‘तद्’ शब्दों के रूप में ‘त’ की जगह ‘ध’ कर देने से ‘यद्’ के रूप बन जाते हैं।
प्रथमा एकवचन में ‘ध’: पुल्लिंग में, ‘या’ स्त्रीलिंग में और ‘यत्’ नपुंसकलिंग में बनते हैं।
यद् (जो) शब्द रूप पुल्लिंग
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | यः | यौ | ये |
| द्वितीया | यम् | यौ | यान् |
| तृतीया | येन | याभ्याम् | यैः |
| चतुर्थी | यस्मै | याभ्याम् | येभ्यः |
| पंचमी | यस्मात् | याभ्याम् | येभ्यः |
| षष्ठी | यस्य | ययोः | येषाम् |
| सप्तमी | यस्मिन् | ययोः | येषु |
नपुंसकलिंग
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | यत् | ये | यानि |
| द्वितीया | यत् | ये | यानि |
| तृतीया | येन | याभ्याम् | यैः |
| चतुर्थी | यस्मै | याभ्याम् | येभ्यः |
| पंचमी | यस्मात् | याभ्याम् | येभ्यः |
| षष्ठी | यस्य | ययोः | येषाम् |
| सप्तमी | यस्मिन् | ययोः | येषु |
स्त्रीलिंग
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | या | ये | याः |
| द्वितीया | याम् | ये | याः |
| तृतीया | यया | याभ्याम् | याभिः |
| चतुर्थी | यस्यै | याभ्याम् | याभ्यः |
| पंचमी | यस्याः | याभ्याम् | याभ्यः |
| षष्ठी | यस्याः | ययोः | यासाम् |
| सप्तमी | यस्याम् | ययोः | यासु |
किम् (कौन) शब्द रूप – पुल्लिंग
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | कः | कौ | के |
| द्वितीया | कम् | कौ | कान् |
| तृतीया | केन | काभ्याम् | कैः |
| चतुर्थी | कस्मै | काभ्याम् | केभ्यः |
| पंचमी | कस्मात् | काभ्याम् | केभ्यः |
| षष्ठी | कस्य | कयोः | केषाम् |
| सप्तमी | कस्मिन् | कयोः | केषु |
किम् (कौन) शब्द रूप नपुंसकलिंग
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | किम् | के | कानि |
| द्वितीया | किम् | के | कानि |
| तृतीया से सप्तमी | — | ➡️ शेष पुल्लिंग के रूप जैसे हैं |
स्त्रीलिंग
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | का | के | काः |
| द्वितीया | काम् | के | काः |
| तृतीया | क्या | काभ्याम् | काभिः |
| चतुर्थी | कस्यै | काभ्याम् | काभ्यः |
| पंचमी | कस्याः | काभ्याम् | काभ्यः |
| षष्ठी | कस्याः | कयोः | कासाम् |
| सप्तमी | कस्याम् | कयोः | कासु |
इदम् (यह) शब्द रूप पुल्लिंग
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | अयम् | इमौ | इमे |
| द्वितीया | एनम् | इमौ | इमान् |
| तृतीया | अनेन | आभ्याम् | एभिः |
| चतुर्थी | अस्मै | — | एभ्यः |
| पंचमी | अस्मात् | — | एभ्यः |
| षष्ठी | अस्य | अनयोः | एषाम् |
| सप्तमी | अस्मिन् | अनयोः | एषु |
नपुंसकलिंग
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | इदम् | इमे | इमानि |
| द्वितीया | इदम् | इमे | इमानि |
| तृतीया से सप्तमी | — | ➡️ शेष पुल्लिंग की तरह |
स्त्रीलिंग
| विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुवचन |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | इयम् | इमे | इमाः |
| द्वितीया | एमम् | इमे | इमाः |
| तृतीया | अनया | आभ्याम् | आभिः |
| चतुर्थी | — | — | आभ्यः |
| पंचमी | अस्याः | — | आभ्यः |
| षष्ठी | — | अनयोः | आसाम् |
| सप्तमी | अस्याम् | अनयोः | आसु |
अस्मद् (मैं, हम)
| विभक्ति | एकवचन (मैं) | द्विवचन (हम दो) | बहुवचन (हम सब) |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | अहम् | आवाम् | वयम् |
| द्वितीया | माम्, मा (मुझको) | आवाम्, नौ (हम दोनों को) | अस्मान्, नः (हमको) |
| तृतीया | मया (मेने) | आवाभ्याम् (हम दोनों ने) | अस्माभिः (हमने) |
| चतुर्थी | मह्यम्, मे (मेरे लिये) | आवाभ्याम्, नौ (हम दोनों के लिये) | अस्मभ्यम्, नः (हमारे लिये) |
| पंचमी | मत् (मुझसे) | आवाभ्याम् (हम दो से) | अस्मात् (हमसे) |
| षष्ठी | मम, मे (मेरा) | आवयोः, नौ (हम दो का) | अस्माकम्, नः (हमारा) |
| सप्तमी | मयि (मुझ पर) | आवयोः (हम दो पर) | अस्मासु (हम पर) |
युष्मद् (तू, तुम)
| विभक्ति | एकवचन (तू) | द्विवचन (तुम दोनों) | बहुवचन (तुम सब) |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | त्वम् | युवाम् | यूयम् |
| द्वितीया | त्वाम्, ता (तुझको) | युवाम्, वाम् (तुम दो को) | युष्मान्, वः (तुमको) |
| तृतीया | त्वया (तूने) | युवाभ्याम् (तुम दोनों ने) | युष्माभिः (तुमने) |
| चतुर्थी | तुभ्यम्, ते (तेरे लिये) | युवाभ्याम्, वाम् (तुम दोनों के लिये) | युष्मभ्यम्, वः (तुम्हारे लिये) |
| पंचमी | त्वत् (तुझसे) | युवाभ्याम् (तुम दो से) | युष्मत् (तुमसे) |
| षष्ठी | तव, ते (तेरा) | युवयोः, वाम् (तुम दोनों का) | युष्माकम्, वः (तुम्हारा) |
| सप्तमी | त्वयि (तुम पर) | युवयोः (तुम दो पर) | युष्मासु (तुम पर) |
विशेषण:
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। इनके लिंग अपने विशेष्यों के अनुसार होते हैं,
जैसे —
सुंदर: बालक (पुल्लिंग) सुन्दरी बालिका (स्त्रीलिंग), सुन्दरम् फलम् (नपुंसकलिंग) में ‘सुन्दर’ विशेषण है, जो अपने विशेष्यों — बालकः, बालिका और फलम् — के अनुसार लिंग बदलता रहता है।
संस्कृत में सर्वनामों का प्रयोग भी विशेषण की भाँति होता है। जैसे—एषः बालकः (यह लड़का) में ‘एषः’ सर्वनाम विशेषण की तरह आया है। विशेषणों की भाँति होने वाले सर्वनामों के रूपों में इस प्रयोग से कोई अन्तर नहीं आता। अन्य विशेषणों के रूप संज्ञा की भाँति चलते हैं, अतः उनके रूप इस प्रकार्य में नहीं लिखे जायेंगे।
संख्यावाचक शब्द रूप
एक (केवल एकवचन)
| विभक्ति | पुल्लिंग | नपुंसकलिंग | स्त्रीलिंग |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | एकः | एकम् | एका: |
| द्वितीया | एकम् | एकम् | एकाम् |
| तृतीया | एकेन | एकेन | एकया |
| चतुर्थी | एकस्मै | एकस्मै | एकस्यै |
| पंचमी | एकस्मात् | एकस्मात् | एकस्याः |
| षष्ठी | एकस्य | एकस्य | एकस्याः |
| सप्तमी | एकस्मिन | एकस्मिन | एकस्याम् |
द्वि-दो (केवल द्विवचन)
| विभक्ति | पुल्लिंग | नपुंसकलिंग | स्त्रीलिंग |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | द्वौ | द्वे | द्वे |
| द्वितीया | “ | “ | “ |
| तृतीया | द्वाभ्याम् | द्वाभ्याम् | द्वाभ्याम् |
| चतुर्थी | “ | “ | “ |
| पंचमी | “ | “ | “ |
| षष्ठी | द्वयोः | द्वयोः | द्वयोः |
| सप्तमी | द्वयोः | द्वयोः | द्वयोः |
नोट — त्रि (तीन) से लेकर अष्टादश (अठारह) तक सभी संख्यावाचक शब्द केवल बहुवचन के होते हैं।
त्रि — तीन (केवल बहुवचन)
| विभक्ति | पुल्लिंग | नपुंसकलिंग | स्त्रीलिंग |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | त्रयः | त्रिणि | तिस्रः |
| द्वितीया | त्रीन | “ | “ |
| तृतीया | त्रिभिः | त्रिभिः | तिसृभिः |
| चतुर्थी | त्रिभ्यः | त्रिभ्यः | तिसृभ्यः |
| पंचमी | त्रिभ्यः | त्रिभ्यः | तिसृभ्यः |
| षष्ठी | त्रयाणाम् | त्रयाणाम् | तिसृणाम् |
| सप्तमी | त्रिषु | त्रिषु | तिसृषु |
चतुर् — चार (केवल बहुवचन)
| विभक्ति | पुल्लिंग | नपुंसकलिंग | स्त्रीलिंग |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | चत्वारः | चत्वारि | चतसः |
| द्वितीया | चत्वारः | चत्वारि | “ |
| तृतीया | चतुर्भिः | चतुर्भिः | चतसृभिः |
| चतुर्थी | चतुर्भ्यः | चतुर्भ्यः | चतसृभ्यः |
| पञ्चमी | “ | “ | “ |
| षष्ठी | चतुर्णाम् | चतुर्णाम् | चतसृणाम् |
| सप्तमी | चतुर्षु | चतुर्षु | चतसृषु |
| विभक्ति | पञ्चन् (पाँच)
तीनों लिंगों में सामान |
षष्ठन् (छः)
तीनों लिंगों में सामान |
सप्तन् (सात)
तीनों लिंगों में सामान |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | पञ्च | षट् | सप्त |
| द्वितीया | “ | “ | “ |
| तृतीया | पञ्चभिः | षड्भिः | सप्तभिः |
| चतुर्थी | पञ्चाय्यः | षड्भ्यः | सप्तभ्यः |
| पंचमी | “ | “ | “ |
| षष्ठी | पञ्चानाम् | षण्णाम् | सप्तानाम् |
| सप्तमी | पञ्चसु | षट्सु | सप्तसु |
| विभक्ति | अष्टन् (आठ)
तीनों लिंगों में सामान |
नवन् (नौ)
तीनों लिंगों में सामान |
दशन् (दस)
तीनों लिंगों में सामान |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | अष्ट, अष्टौ | नव | दश |
| द्वितीया | अष्ट, अष्टौ | नव | दश |
| तृतीया | अष्टभिः, अष्टाभिः | नवभिः | दशभिः |
| चतुर्थी | अष्टभ्यः, अष्टाभ्यः | नवभ्यः | दशभ्यः |
| पंचमी | “ | “ | “ |
| षष्ठी | अष्टानाम् | नवानाम् | दशानाम् |
| सप्तमी | अष्टसु, अष्टासु | नवसु | दशसु |
कति (कितने)
संख्यावाची ‘कति’ शब्द के रूप भी तीनों लिंगों में समान और हमेशा बहुवचन में होते हैं।
| विभक्ति | रूप |
|---|---|
| प्रथमा | कति |
| द्वितीया | कति |
| तृतीया | कतिभिः |
| चतुर्थी | कतिभ्यः |
| पंचमी | “ |
| षष्ठी | कतिनाम् |
| सप्तमी | कतिषु |
विशेष:
- विशेषण के प्रयोग में एक से चार तक के शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में भिन्न-भिन्न होता है।
- पाँच से उन्नीस तक शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में एक-सा होता है।
1 से 100 तक संस्कृत संख्यावाचक शब्द
१. एकः, एकम्, एका
२. द्वौ, द्वे, द्वे
३. त्रयः, त्रीणि, तिस्रः
४. चत्वारः चत्वारि, चतस्रः
५. पञ्च (चार के आगे तीनों लिंगों में एक ही रूप होता है ।)
६. षट्
७. सप्त
८. अष्ट, अष्टौ
९. नव
१०. दश
११. एकादश
१२. द्वादश
१३. त्रयोदश
१४. चतुर्दश
१५. पञ्चदश
१६. षोडश
१७. सप्तदश
१८. अष्टादश
१९. एकोनविंशतिः, नवदश
२०. विंशतिः
२१. एकविंशतिः
२२. द्वाविंशतिः
२३. त्रयोविंशतिः
२४. चतुर्विंशतिः
२५. पञ्चविंशतिः
२६. षड्विंशतिः
२७. सप्तविंशतिः
२८. अष्टाविंशतिः
२९. एकोनविंशतिः
३०. त्रिंशत्
३१. एकत्रिंशत्
३२. द्वात्रिंशत्
३३. त्रयत्रिंशत्
३४. चतुस्त्रिंशत्
३५. पञ्चत्रिंशत्
३६. षट्त्रिंशत्
३७. सप्तत्रिंशत्
३८. अष्टात्रिंशत्
३९. एकोनचत्वारिंशत्, नवत्रिंशत्
४०. चत्वारिंशत्
४१. एकचत्वारिंशत्
४२. द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्
४३. त्रिचत्वारिंशत्
४४. चतुश्चत्वारिंशत्
४५. पञ्चचत्वारिंशत्
४६. षट्चत्वारिंशत्
४७. सप्तचत्वारिंशत्
४८. अष्टाचत्वारिंशत्
४९. एकोनचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्
५०. पञ्चाशत्
५१. एकपञ्चाशत्
५२. द्विपञ्चाशत्, द्वापञ्चाशत्
५३. त्रिपञ्चाशत्, त्रयः पञ्चाशत्
५४. चतुः पञ्चाशत्
५५. पञ्चपञ्चाशत्
५६. षटपञ्चाशत्
५७. सप्तपञ्चाशत्
५८. अष्टापञ्चाशत्, अष्टपञ्चाशत्
५९. एकोनषष्टि, नवपञ्चाशत्
६०. षष्टिः
६१. एकषष्टिः
६२. द्विषष्टि, द्वाषष्टिः
६३. त्रिषष्टिः, त्रयष्षष्टिः
६४. चतुष्षष्टिः
६५. पञ्चषष्टिः
६६. षट्षष्टिः
६७. सप्तषष्टिः
६८. अष्टषष्टिः, अष्टाषष्टिः
६९. एकोनसप्ततिः, ऊनसप्ततिः नवषष्टि
७०. सप्ततिः
७१. एकसप्ततिः
७२. द्विसप्तति, द्वासप्ततिः
७३. त्रयसप्तति, त्रयस्तप्ततिः
७४. चतुस्सप्ततिः
७५. पञ्चसप्ततिः
७६. षट्सप्ततिः
७७. सप्तसप्ततिः
७८. अष्टसप्ततिः, अष्टासप्ततिः
७९. एकोनाशीतिः, ऊनशीतिः नवसप्ततिः
८०. अशीतिः
८१. एकशीतिः
८२. द्वयशीतिः
८३. त्रयशीतिः
८४. चतुरशीतिः
८.५. पञ्चाशीतिः
८६. षड्शीतिः
८७. सप्तशीतिः
८८. अष्टाशीतिः
८९. एकोननवतिः नवशीतिः
९०. नवतिः
९१. एकनवतिः
९२. द्विनवतिः द्वानवतिः
९३. त्रिनवतिः, त्रयोनवतिः
९४. चतुर्नवतिः
९५. पञ्चनवतिः
९६. षष्णवतिः
९७. सप्टनवतिः
९८. अष्टनवतिः, अष्टानवति
९९. एकोनशतम्, नवनवतिः
१००. शतम्
हजार = सहस्रम्
दस हजार = अयुतम्
लाख = लक्षम्
दस लाख = प्रयुतम्, नियुतम्
करोड़ = कोटिः
दस करोड़ = दश कोटि
अरब = अर्बुदम्
दस अरब = दशार्बदम्
खरब = खर्बम्
दस खरब = दश खर्बम्
नील = नीलम्
दस नील = दश नीलम्
पद्म = पदमम्
दस पदम् = दश पदमम्
शंख = शंखम्
दस शंख = दश शंखम्
महाशंख = महाशंखम्
शब्द रूप याद रखने के कुछ साधारण नियम
शब्द के लिंग तथा अन्तिम स्वर अथवा व्यंजन के अनुसार शब्दों के रूप चलते हैं। यद्यपि ये सम्पूर्ण रूप निश्चित नियमों के अनुसार ही चलते हैं, पर ये नियम इतने अधिक हैं कि सामान्य छात्रों का उन नियमों के बिना ही रूपों को जान लेना सरल होता है। कुछ साधारण नियम’ नीचे लिखे जाते हैं-
१. नपुंसकलिंग के केवल अकारान्त तथा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के सम्पूर्ण शब्दों के द्वितीया एकवचन के अन्त में ‘म्’ आता है।
२. सर्वनाम, संख्यावाचक, विशेषण और अकारान्त पुल्लिंग शब्द को छोड़कर अन्य शब्दों के पंचमी और षष्ठी एकवचन एक-से होते हैं।
३. प्रायः प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन तथा षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन एक-से होते हैं।
४. सम्बोधन के द्विवचन और बहुवचन प्रायः प्रथमा के द्विवचन और वहुवचन के समान होते हैं।
५. प्रायः चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन एक-से होते हैं, षष्ठी के बहुवचन के अन्त में अधिकतर ‘नाम’ या ‘णाम्’ आता है। सप्तमी के बहुवचन के अन्त में ‘सु’ अथवा ‘षु’ का प्रयोग होता है।
६. अकारान्त पुल्लिंग शब्द के प्रथमा एकवचन में अकारान्त शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों में पंचमी और षष्ठी के एकवचन तथा द्वितीया बहुवचन में विसर्ग शब्दों के अन्त में लगता है।
७. नपुंसकलिंग में प्रथमा तथा द्वितीया के रूप समान होते हैं। अन्य विभक्तियों के रूप प्रायः पुल्लिंग के समान चलते हैं।
८. प्रायः सम्पूर्ण सर्वनामों के रूप एक समान चलते हैं।
विशेष-१. ऊपर के नियमों के अपवाद भी होते हैं। अतः किसी शब्द के रूपों को एक बार ध्यान से देखकर उन अपवादों को समझ लेना चाहिए।
२. रूपों का स्मरण करने का सरल तरीका भी यही है कि पहले किसी एक शब्द या धातु को अच्छी प्रकार समझकर कण्ठस्थ कर लिया जाये, फिर अन्य शब्दों को या धातुओं के रूपों को समझते समय पहले वाले रूपों से मिलाकर उनके अन्तर को समझ लिया जाये।
३. नवीन शब्दों के रूपों को बनाने से पहले यह देख लेना चाहिए कि शब्द का क्या लिंग है और उनके अन्त में कौन-सा स्वर अथवा व्यंजन है, फिर उसी लिंग के उसी स्वर के व्यंजन को अन्त में रखने वाले शब्द के अनुसार उसके रूप चला लेना चाहिए। जैसे- ‘राम’ शब्द का ‘षष्ठी’ के ‘एकवचन’ का रूप ज्ञात करना है। ‘राम पुल्लिंग’ है और उसके अन्त में ‘अ’ है अतः पुल्लिंग में ‘अ’ अन्त में रखने वाले बालक का षष्ठी का एक वचन ‘बालकस्य’ को ध्यान में रखकर राम का ‘रामस्य’ रूप ज्ञात कर लिया ।